सफलता का आधार: उद्यमशीलता
चाणक्य भारतीय राजनीति के पटल पर सदैव एक दृ़ढ़ निश्चयी उद्यमी के तौर पर याद किये जाते रहेंगे। यही नहीं अर्थशास्त्र में भी उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने न केवल उद्यमिता के महत्व को समझा वरन् उद्यमिता के द्वारा ही भारत के इतिहास को ही बदल दिया। चाणक्य स्वयं उद्यमी व्यक्ति थे, तभी तो चाणक्य उद्यमिता को प्रोत्साहित करते हुए लिखते हैं-
उद्योगे नास्ति दारिद्रयं जपतो नास्ति पातकम्।
मौने च कलहो नास्ति, नास्ति जागरिते भयम्।।11!!
चाणक्य नीति के तीसरे अध्याय के इस ग्यारहवे श्लोक में उद्यमिता के महत्व को स्पष्ट किया है। चाणक्य स्वयं भी अच्छे उद्यमी थे। अपनी उद्यमिता के बल पर ही तो उन्होंने भारत के इतिहास में अप्रतिम स्थान पाया। उद्यम अर्थात निरंतर परिश्रम ही गरीबी हटाने का अचूक उपाय है। परिश्रमी व्यक्ति कभी निर्धन नहीं रह सकता। इस श्लोक का आशय है कि जहाँ उद्योग है वहाँ दरिद्रता नहीं हो सकती; जहाँ ईश्वर का ध्यान करते हुए कार्य को संपन्न किया जाता है वहाँ पाप नहीं हो सकता; जहाँ मौन रखा जाय वहाँ कलह नहीं हो सकती और जाग्रत रहने पर किसी भी प्रकार का भय नहीं हो सकता।
गीता में भी उद्यमशीलता या कर्म पर जोर देते हुए कहा गया है कि तेरा कर्म पर अधिकार है। तू फल की चिंता किये बिना कर्म कर। फल की चिंता किए बिना कर्म करने की अभिप्रेरणा हमें अपने कर्म पर एकाग्रचित्त रहने को प्रोत्साहित करती है-
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते संगोऽस्त्वकर्मणि।।
तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मो के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। इस श्लोक में ये नहीं कहा गया है कि कर्म का फल नहीं मिलेगा। कर्म का फल तो प्रकृति के नियमों के अनुसार अवश्य ही मिलेगा, क्योंकि जहाँ कारण होगा कार्य भी होगा।
जब हम काम करते समय उसके परिणाम का चिंतन करते हैं तो काम को अपना संपूर्ण नहीं दे पाते और जब हम शत-प्रतिशत लगायेंगे ही नहीं तो अच्छे परिणाम कहाँ से प्राप्त होंगे। यदि विद्यार्थी अध्ययन के समय परीक्षा के बारे में विचार करेगा तो वह सही ढंग से सीख नहीं पायेगा। अतः उसे सीखने पर ही ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। यदि वह विषय पर अधिकार कर लेगा तो परीक्षाएँ तो अपने आप ही अच्छी होंगी।
अतः हमें करना केवल इतना है कि परिणाम या फल के प्रति आसक्ति का त्याग करना है। हमको धन का त्याग नहीं करना है, धन के प्रति आसक्ति का त्याग करना है। घर-बार छोड़कर जंगलों में नहीं जाना है, केवल आसक्ति को त्याग कर सभी के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना है। अध्यात्म में कंचन और कामिनी को छोड़ने की बात की जाती है। वस्तुतः न तो कंचन को छोड़ने की आवश्यकता है और न ही कामिनी को इन दोनों के बिना सृष्टि व्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती और कोई भी नियम धर्म का अंग नहीं हो सकता जो प्रकृति के नित्य क्रम को ही बाधित करे। वस्तुतः कंचन और कामिनी को नहीं इनके प्रति आसक्ति को त्यागना है। कर्म को नहीं त्यागना, फल को भी नहीं त्यागना, फल की आसक्ति को त्यागना है। हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन परिणामों की आकांक्षा किए बिना करना है। आधुनिक प्रबंध विज्ञान के समस्त तरीके इसी आधार पर स्पष्ट किये जा सकते हैं। कार्य प्रबंधन, तनाव प्रबंधन व जीवन प्रबंधन गीता के द्वारा किया जा सकता है।
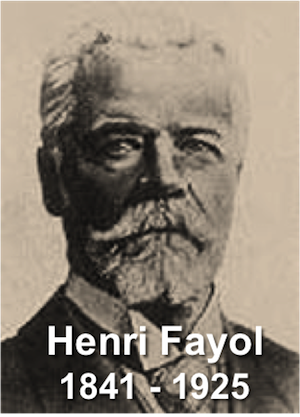





कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें