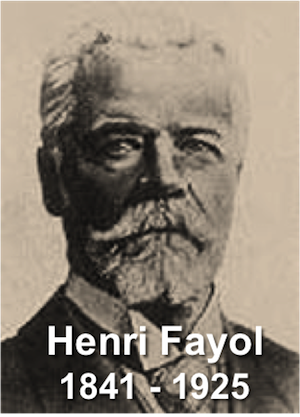कार्य प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्र
मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में समय के संदर्भ में कार्य प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। समय सर्वव्यापक है। संपूर्ण संसार में समय ही है जो अनादि, अनन्त और क्षणभंगुर है। समय अपने आप में असीम व अनन्त है किंतु मानव ही क्यों? अमानवीय साधनों का भी निर्धारित जीवन काल होता है। समय अपने आप में असीम व अनंत भले ही हो, हमारे पास असीमित समय नहीं है। हम यह तो जानते हैं कि हमें प्राप्त समय सीमित है किंतु कितना सीमित है? हम तो उस सीमा को भी नहीं जानते। अगले क्षण भी हम जीवित रहेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं ले सकता। इसीलिए जीवन को क्षणभंगुर कहा जाता है, अर्थात सभी मानवीय व अमानवीय संसाधन क्षणभंगुर हैं। कब नष्ट होकर दूसरे रूप में आ जायँ? कोई नहीं जानता। समय अनादि है, जिसका आदि अर्थात् प्रारंभ कब हुआ हम नहीं जानते। समय अनन्त है अर्थात् इसका अंत नहीं होगा किंतु हमारे लिए यह क्षणभंगुर है क्योंकि हमारा समय कब समाप्त हो जायेगा? हम नहीं जानते। इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि हमारे शरीर सहित सभी पदार्थ क्षणभंगुर हैं। इस अनिश्चित समय में ही हमें व्यक्तिगत, पारिवारिक व सामाजिक अनेक काम करने हैं। इन अनेक कार्यो का उपलब्ध समय के सन्दर्भ में प्रबंधन करना अत्यावश्यक है।
जीवन भले ही क्षणभंगुर हो किंतु हमारे कर्तव्य असीमित होते हैं। हम अपनी मृत्यु के बाद तक के लिए अपने लोगों के लिए व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं। हमारे पास कामों की कमी कभी नहीं होती। एक समाप्त होता है, चार प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। अर्थशास्त्र में चयन के सिद्धांत के अनुसार विकल्प अनेक होते हैं तो चयन करना पड़ता है। यही तो प्रबंधन में निर्णयन कहलाता है। चयन का मतलब अपने कार्यो की प्राथमिकताओं का निर्धारण करना, प्रस्तावित कार्य के लिए समय का आवंटन करना और उस समय में कार्य को पूर्ण प्रभावशीलता के साथ पूर्ण करने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। इसे सामान्यतः कार्य प्रबंधन कहा जाता है किंतु वास्तव में समय का प्रबंधन नहीं हो सकता। अतः हम इसे कार्य प्रबंधन कहना ही उपयुक्त समझते हैं।
हमें हर क्षेत्र में समय की कमी महसूस होती है। अधिकांश व्यक्ति समय की कमी का रोना रोते देखे जा सकते हैं। इसी कारण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। कार्य प्रबंधन में कुशलता या अकुशलता ही सफलता या असफलता का आधार होती है। फील्ड के अनुसार, ‘सफलता और असफलता के बीच की सबसे बड़ी विभाजक रेखा को इन पाँच शब्दों में बताया जा सकता है कि ‘मेरे पास समय नहीं है।’’ वास्तव में सभी के पास समय है। यह उस पर निर्भर करता है कि वह अपने समय को कहाँ और किस प्रकार उपयोग करता है? यह समय के संदर्भ में अपनी गतिविधियों के प्रबंधन पर निर्भर करता है। अपनी प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। कार्य प्रबंधन को विभिन्न क्षेत्रों में लागू करके ही सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। विभिन्न क्षेत्रों में कार्य प्रबंधन की आवश्यकता को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है।
सभी क्षेत्रों में प्रबंधन की आवश्यकताः
संसार में समस्त कार्य समय के संदर्भ में प्रबंधन की माँग करते हैं। कार्य प्रबंधन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उपयोगी रहता है, किसी घर का प्रबंध सभालने वाली सामान्य गृहिणी हो, किसान हो, मजदूर हो, कोई डाक्टर हो, कोई छोटा-मोटा व्यापारी हो, कोई बड़ा उद्योगपति हो, पेशेवर चार्टर्ड एकाउटेण्ट, वकील ही क्यों न हो सभी को कार्य प्रबंधन की आवश्यकता होती है। सभी कुछ न कुछ मात्रा में प्रबंधन करते ही हैं। उनकी प्रबंध कुशलता ही उनके स्तर को निर्धारित करती है। जिसमें जितनी अधिक प्रबंध कुशलता होती है, वह उतना ही अधिक महत्वपूर्ण कार्य करने व करवाने में सफल होता है। प्रबंध कुशलता में सक्षम व्यक्ति के लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं होता। कोई व्यक्ति किसी छोटे से छोटे कार्य को कर रहा हो या बड़े से बड़े कार्य करने में व्यस्त हो किंतु उसे प्रबंधन तो करना ही होता है। प्रबंधन ही उस कार्य को पूर्णता दिलाता है।
एक छोटे बच्चे को भी अपने प्रिय खेल में भाग लेने के लिए माता के हाथ के दूध को छोड़कर भाग जाना पड़ता है। आप किसी निठल्ले बैठे व्यक्ति को कोई रचनात्मक कार्य बतायेंगे तो वह भी यही कहेगा कि उसके पास समय नहीं है। उसके द्वारा यह कहने का आशय यह नहीं है कि उसके पास समय नहीं है। उसका आशय यह है कि उसने अपने लिए प्राथमिकताओं का निर्धारण कुछ अलग ढंग से कर रखा है। उसे उस समय को कहीं अन्यत्र लगाना है। हम यह कह सकते हैं कि उसने अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण सही से नहीं किया है और अपनी गतिविधियों का समय के संदर्भ में प्रबंधन करना उसे नहीं आता है, किंतु उसके विचार व योग्यता के अनुसार वही सही है। सभी व्यक्तियों को सभी क्षेत्रों में प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के सन्दर्भ में कार्य प्रबंधन की चर्चा करना उपयोगी रहेगा।
1. गृहिणी के लिए कार्य प्रबंधन की आवश्यकता-
व्यक्ति के जीवन में प्रथम समूह उसका घर अर्थात्् परिवार होता है। परिवार का मुख्य आधार गृहिणी होती है। कहावत भी है, ‘बिन घरनी, घर भूत का डेरा’। परिवार का सृजन, विकास व परिवर्धन गृहिणी के द्वारा ही संभव है। गृहिणी द्वारा गृह प्रबंधन कुशलता के साथ हो तो घर ही जन्नत बन जाता है। यदि गृहिणी गृह प्रबंध में कुशल न हो या उसकी निष्ठा घर से बाहर हो तो घर -घर नहीं रहता, एक भवन मात्र रह जाता है, ऐसे भवन को नर्क या दोजख में परिवर्तित होने में अधिक समय नहीं लगता। महत्त्वाकांक्षी व कर्मठ व्यक्ति के लिए ऐसा घर प्रताड़ना भवन बन जाता है और ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसे घर से अलग हो जाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहता।
इस प्रकार मेरे कहने का आशय यह है कि परिवार व्यक्तित्व के विकास व समाज का आधार होता है और गृहिणी घर का आधार होती है। संपूर्ण घर को कुशलता के साथ संभालने के लिए गृहिणी को कार्य प्रबंधन की अत्यन्त आवश्यकता होती है। एक घर-गृहस्थी को कुशलतापूर्वक संभालने वाली महिला भी एक प्रबंधक है और किसी संस्था को संभालने वाले प्रबंधक से किसी भी प्रकार से कम नहीं होती। किसी संस्था के प्रबंधक के कत्र्तव्य पूर्णतः परिभाषित होेते हैं। एक गृहिणी के कत्र्तव्य और उत्तरदायित्व परिभाषित नहीं होते, असीमित होते हैं।
गृहिणी को न केवल घर का प्रबंधन करना होता है, वरन् उसे संबन्धों का प्रबंधन भी करना होता है, अपने आप का भी प्रबंधन करना होता है। वह ही एकमात्र धुरी होती है जो सभी परिवारीजनों को एक सूत्र में बांधे रखती है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए उसके पास समय की कमी बराबर बनी रहती है किंतु इसके बाबजूद वह कार्य प्रबंधन तकनीकों का प्रयेाग करके सब कुछ व्यवस्थित बनाये रखने में सफल होती है।
वह परिवारीजनों से बिना किसी आधिकारिकता के सहयोग लेती है। बच्चों से सहयोग लेती है, बड़ों से सहयोग लेती है, सभी को प्रसन्न रखने की कोशिश करती है और सभी की प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता खोज लेती है। इतनी महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन वह कार्य प्रबंधन के द्वारा ही कर पाने में सफल होती है। निःसन्देह एक घर को चलाने का कार्य एक संस्था के चलाने के कार्य से अधिक प्रबंध कुशलता की मांग करता है।
अतः हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि एक गृहिणी कार्य प्रबंधन के द्वारा ही अपने उत्तरदायित्वों का कुशलता व सफलता के साथ निर्वहन कर पाती है। हाँ! यह अलग बात है कि उसे कार्य प्रबंधन के शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए किसी विद्यालय या महाविद्यालय में नहीं जाना पड़ता। पारंपरिक रूप से अपने घर से ही वह प्रबंधन में कुशलता हासिल कर लेती है। धीरे-धीरे यह पक्ष कमजोर पड़ता जा रहा है, गृह प्रबंधन सीखने की पारंपरिक व्यवस्था कमजोर पड़़ती जा रही है। अतः हो सकता है, अगली शताब्दी में गृह प्रबंधन भी एक स्वतंत्र विषय के रूप में विद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ाना प्रारंभ करना पड़े।
2. विद्यार्थियों के लिए कार्य प्रबंधन की आवश्यकता:-
विद्यार्थी किसी भी देश की पूँजी होते हैं। विद्यार्थियों को किसी भी देश का भविष्य कहा जाता है। ‘अध्यापक हैं युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता’ नारे के अनुसार; उन्हें राष्ट्र का भाग्य विधाता भी कहा जाता है। विद्यार्थी जीवन सबसे अधिक मजेदार और भविष्य की तैयारी के लिए सबसे अधिक उत्तरदायित्व वाला काल होता है। विद्यार्थियों को अध्ययन ही नहीं, व्यक्तिगत, पारिवारिक, विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों, पाठ्येत्तर गतिविधियों व अन्य अनेक गतिविधियों में व्यस्त रहना होता है। व्यक्तिगत स्तर पर भी विद्यार्थी जीवन को ही मौजमस्ती का काल भी कहा जाता रहा है। वर्तमान में कैरियर को लेकर विद्यार्थी मनोवैज्ञानिक दबाव में भी रहते हैं। विद्यार्थी को अभिभावकों की अति महत्त्वाकांक्षा के दबाव का भी सामना करना पड़ता है।
विद्यार्थियों को प्रातःकाल पीटी से लेकर, कक्षाओं के नियमित कालांशों के अलावा सायंकालीन खेलकूद में भी भाग लेना होता है। विद्यालय समय के बाद भी कक्षाओं में ढेर सारा गृहकार्य भी दे दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त कक्षाओं की भी परंपरा चल पड़ी है। इस प्रकार विद्यार्थी भी बहुत अधिक व्यस्त हो जाता है। कई विद्यार्थी तो अवसाद के शिकार हो जाते हैं। ऐसी स्थितियों में अपनी सभी गतिविधियों में सफलतापूवर्क भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को अपनी सभी गतिविधियों का समय के सन्दर्भ में प्रबंधन करना पड़ता है। समय के सन्दर्भ में कार्य प्रबंधन ही विद्यार्थियों को तनाव, दबाब व अवसाद से बचाकर सफलता दिलाने का एकमात्र विकल्प है।
कार्य प्रबंधन के बिना विद्यार्थी जीवन की सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। विद्यार्थी का संपूर्ण जीवन समय तालिका के अनुसार विद्यालय की घण्टियों पर चलता है। विद्यार्थी जीवन में ही व्यक्ति बार-बार समय तालिका बनाने और लागू करने का प्रयास करता है। यदि वह अपनी समय तालिका को भली प्रकार बना और लागू कर पाता है तो ज्ञान की उपलब्धियाँ हासिल कर सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी जीवन के लिए कार्य प्रबंधन अत्यन्त आवश्यक है। इसी काल में वह समय के सन्दर्भ में कार्य प्रबंधन सीखने का अभ्यास भी करता है।
3. व्यापारियों के लिए कार्य प्रबंधन की आवश्यकता:-
किसी भी कार्य को करने के लिए समय के अनुशासन की आवश्यकता रहती है। क्रय व विक्रय की क्रिया से लाभ कमाने को व्यापार कहते हैं। व्यापार तो समय पालन पर ही निर्भर करता है। जो व्यक्ति समय पालन नहीं कर सकता, वह कभी भी अच्छा व्यापारी क्या? व्यापारी ही नहीं हो सकता। समय के अनुशासन का पालन करके ही वह अपने ग्राहकों का विश्वास अर्जित कर सकता है। समय के सन्दर्भ में व्यापारिक गतिविधियों का प्रबंधन किए बिना व्यापार की साख निर्मित नहीं हो सकती और कोई भी व्यापार साख के बिना दीर्घकाल तक चल ही नहीं सकता।
व्यापारी अपने व्यवसाय का स्वयं मालिक होता है, अतः संपूर्ण व्यापार के संचालन का उत्तरदायित्व उसी का होता है। उसे अन्य व्यक्तियों से भी काम लेना होता है। उसके व्यापार में अन्य संसाधनों का भी निवेश होता है। व्यापारी के लिए समय का अत्यन्त महत्त्व है। अधिक समय तक उधारी रहने पर व्यापारी एक-एक दिन का ब्याज लगा लेता है। व्यापारी को अपने ही नहीं, अपने कर्मचारियों व अन्य आर्थिक संसाधनों के समय का भी प्रबंधन करना होता है।
4. उद्योगपतियों के लिए कार्य प्रबंधन की आवश्यकता:-
उद्यम को करने वाले उद्यमी कहलाते हैं। उद्यम ही आधुनिक औद्योगिक विकास की धुरी है। उद्योग के अन्तर्गत अधिकांशतया वस्तुओं का उत्पादन, निर्माण या प्रक्रियाकरण सम्मिलित होता है। उद्योग किसी देश के विकास की आधारशिला होते हैं। उद्यमी छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। बड़ा होने पर वही उद्योगपति कहलाता है। उद्योगपति ही देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। उद्योगपति पूँजी लगाते हैं, इसी कारण इन्हें पूँजीपति भी कहते हैं।
पेशेवर प्रबंधन का श्रेय पूँजीपतियों को ही जाता है। जब तक उद्योग व व्यवसाय छोटे स्तर पर रहता है, मालिक ही प्रबंधक का काम भी करते हैं। जब उत्पादन बड़े पैमाने पर करने के लिए वृहद स्तर के उद्योगों की स्थापना की जाती है। वृहद स्तर के उद्योग काॅरपोरेशन प्रारूप में काम करते हैं। कम्पनी प्रारूप में स्वामित्व और प्रबंधन अलग-अलग होते हैं।
उद्योगपति उद्योग का प्रबंधन स्वयं नहीं करते हैं, पेशेवर प्रबंधकों से करवाते हैं। पेशेवर प्रबंधक ही वास्तव में उद्योगों का संचालन करते हैं। उद्योगपति पेशेवर प्रबंधकों से प्रबंधन करवाते हैं। इसका आशय यह नहीं है कि उद्योगपतियों पर कोई काम नहीं होता। पेशेवर प्रबंधकों से काम करवाने के लिए भी काम करना पड़ता है। दूसरों से कार्य करवाना ही तो प्रबंधन है। ‘कार्य करने वाला व्यक्ति कर्मचारी होता है, किंतु काम करवाने वाला व्यक्ति प्रबंधक होता है।’ काम करवाने के लिए भी प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। उद्योगपति कार्य प्रबंधन करके ही पूँजीपति बनते हैं। कार्य प्रबंधन के बिना वे उद्योगपति रहेंगे ही नहीं। इस प्रकार उद्योगपति को भी कदम-कदम पर कार्य प्रबंधन पर ध्यान दे देना चाहिए। वास्तव में उद्यमी प्रबंधकों का भी प्रबंधक होता है। कार्य प्रबंधन के बिना वह एक साथ अनेक उद्यमों का स्वामित्व सभांल पाने में सक्षम न हो सकेगा। अतः उद्यमियों के लिए समय के संदर्भ में कार्य प्रबंधन अनिवार्य है।
5. फ्रीलांसरों के लिए कार्य प्रबंधन की आवश्यकता:-
जो व्यक्ति किसी के अधीन कार्य न करके स्वतंत्र रूप से अपनी क्षमता व कुशलता के साथ कार्य करते हैं, उन्हें फ्रीलांसर कहते हैं। फ्रीलांसर अधिकांशतया अपने घर से ही कार्य करते हैं। उनका घर ही उनका कार्यालय हो सकता है, आवश्यकता के अनुसार घर से अलग कार्यालय की भी स्थापना कर सकते हैं। ये अपनी सेवाएं विभिन्न बाहरी पार्टियों को प्रदान करते हैं और कार्य के आधार पर भुगतान प्राप्त करते हैं। घर से कार्य करते हुए अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक व अपने व्यावसायिक कत्र्तव्यों को एक साथ पूरा करना काफी कठिन होता है। इस कठिन कार्य को पूरा करने के लिए फ्रीलांसर को अनिवार्यतः कार्य प्रबंधन करना ही होता है। फ्रीलांसर कार्य प्रबंधन को अपनाये बिना कभी अपने हुनर को निखार नहीं सकता। उसे अपने सभी कार्य समयनिष्ठ रहकर पूरे करने होते हैं।
6. विभिन्न पेशेवरों के लिए कार्य प्रबंधन की आवश्यकता:-
वर्तमान समय में न केवल पारंपरिक पेशों का विकास हो रहा है, वरन् नये-नये पेशों का भी जन्म हो रहा है। कोई भी पेशा विशिष्टीकृत सेवाओं का विक्रय है। पेशा व्यक्तिगत आस्था, विश्वास और निष्ठा के आधार पर विकसित और पल्लवित होता है। पेशेवर व्यक्ति को अपनी छवि पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। आस्था, विश्वास और निष्ठा तो समय के अनुशासन से ही पैदा होते हैं। आस्था, विश्वास और निष्ठा के बिना केवल विशिष्टीकृत सेवाओं के बल पर कोई पेशेवर अपने पेशे में सफल नहीं हो सकता।
इस प्रकार कहा जा सकता है कि निष्ठा, आस्था और विश्वास ही वह शक्ति है, जो पेशेवरों को समयनिष्ठ बनाती है। पेशेवरों को समय निष्ठ होना अत्यन्त आवश्यक है अन्यथा वह अपने ग्राहकों का विश्वास अर्जित नहीं कर पाएगा। विश्वास के बिना पेशेवरों की कोई कीमत नहीं रहती। स्पष्ट है किसी भी पेशे के लिए समय के सन्दर्भ में कार्य प्रबंधन अत्यन्त आवश्यक है।
7. प्रबंधकों व प्रशासकों के लिए कार्य प्रबंधन की आवश्यकता:-
प्रबंधक व प्रशासक किसी भी संस्था के संचालक होते हैं। संस्था के लिए नीतियों को विकसित करने से लेकर उन्हें लागू करके सफलतापूर्वक संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने का सारा उत्तरदायित्व प्रबंधकों और प्रशासकों का ही होता है। किसी संस्था का नियोजन, संगठनीकरण, कर्मचारीकरण, निर्देशन व नियंत्रण का संपूण कार्य प्रबंधन व प्रशासन के अन्तर्गत ही आता है। प्रबंधन और प्रशासन में सीमा रेखा खींचकर अन्तर करना भी बड़ा मुश्किल कार्य है। यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
प्रबंधक व प्रशासक ही किसी संस्था की गतिविधियों के लिए जवाबदेह होते हैं। ये संस्था के अन्य सभी वर्गो से अधिक व्यस्त रहते हैं। इनके पास इतने अधिक कार्य होते हैं कि समय के सन्दर्भ में कार्यो का प्रबंधन किए बिना अपने कार्यों को कर ही नहीं सकते। कार्य करने वाले को कर्मचारी कहा जाता है, किंतु अधिक कार्य करने वाले को अधिकारी कहा जाता है। प्रबंधक और प्रशासक, वे अधिकारी है कि वे अधिक कार्य ही नहीं करते, सभी कार्यो को संपन्न करवाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रबंधन व प्रशासन के लिए कार्य प्रबंधन अनिवार्य आवश्यकता है।
8. नेताओं के लिए कार्य प्रबंधन की आवश्यकता:-
वर्तमान समय में नेताओं के लिए नकारात्मक अवधारणा निर्मित होती जा रही है, किंतु हमें विचारने की बात है कि सभी नेता स्वार्थी और लालची नहीं होते। वास्तव में नेता प्रबंधन और प्रशासकों से भी काम करवाने वाला व्यक्ति होता है। नेता वह होता है, जो अपने कामों के माध्यम से बड़े जनसमूह को प्रभावित करता है और जनसमूह की आकांक्षा की पूर्ति के लिए काम करता है। पीटर ड्रकर के अनुसार, ‘प्रबंधक का काम है काम को सही करने का और नेतृत्वकर्ता का काम है सही काम करने का।’
नेताओं को प्रबंधन व प्रशासन से भी अधिक जवाबदेह होना होता है, वे संपूर्ण राष्ट्र व समाज के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कुछ नकारात्मक छवि के नेताओं के कारण हम नेताओं के महत्व व उनके कार्यो को नजर अंदाज नहीं कर सकते। हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ही उदाहरण लें, उन पर अक्सर अधिक विदेश यात्राएँ करने का आरोप लगाया जाता रहा है। इस प्रकार के आरोप लगाने वाले विरोधी नेता वे होते हैं, जो अक्सर अपनी विदेश यात्राओं में आराम फरमाते हैं और केवल निजी पर्यटन के लिए अपनी विदेश यात्राओं का प्रयोग करते हैं। श्री मोदी जी की दिनचर्या संपूर्ण विश्व के लिए एक आदर्श दिनचर्या है। विश्व के नेता भी उनका लोहा मानते हैं।
श्री मोदी जहाँ भी जाते हैं, अपने पास उपलब्ध समय में अपने कार्यक्रमों का प्रबंधन इस प्रकार करते हंै कि वे उस क्षेत्र के अधिकतम् देशों की यात्राएँ कर सकें। अधिकतम् देशों के प्रतिनिधियों से मिल सकें। यहाँ तक कि वे विमान में भी कार्यो को निपटा रहे होते हैं। जहाँ तक जानकारी उपलब्ध है वे 3 से 4 घण्टे का ही विश्राम करते हैं और उनका सारा समय इस प्रकार से आबंटित होता है कि वे अधिकतम् गतिविधियों में भाग ले सकें। विश्व स्तर पर देखने पर अनेक ऐसे नेता मिल जायेंगे जिन्होंने कम समय में प्रबंधन के बल पर प्रभावपूर्ण कार्य किया और कार्य प्रबंधन के क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ गए।
इस प्रकार स्पष्ट है कि समय के संदर्भ में प्रबंधन के असीम क्षेत्र हैं। प्रबंधन, प्रशासन, पेशेवर, उद्यमी, नेता, वकील, अध्यापक, दुकानदार, विद्यार्थी, गृह प्रबंधन, समारोह प्रबंधन आदि कोई भी मानवीय क्रिया ऐसी नहीं है जिसमें समय के सन्दर्भ में प्रबंधन की आवश्यकता न पड़ती हो। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, जहाँ उसे कार्य प्रबंधन की आवश्यकता न पड़ती हो। मनुष्य को जहाँ भी कोई कार्य करना है या करवाना है किसी संसाधन का प्रयोग करना है या करवाना है, वहाँ समय के सन्दर्भ में उसको उन समस्त गतिविधियों का प्रबंधन करना ही होगा। आबंटित व्यक्तियों या वस्तुओं के समय के प्रबंधन के बिना हम उनका मितव्ययितापूर्ण उत्पादक उपयोग सुनिश्चित नहीं कर सकते। अतः कार्य प्रबंधन मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनिवार्य है।