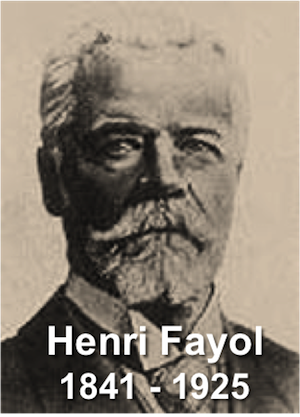चौधराइन अनूठी और अप्रतिम व्यक्तित्व की धनी महिला थीं। जो है, सो है; उन्हें कहने में कोई संकोच न होता। वे स्पष्टवादी अवश्य थीं, किंतु मुँहफट नहीं थीं। ईमानदार लोगों से संसार डरता है। उनके साथ भी मौहल्ले में ऐसा ही व्यवहार था। मैं उनको चौधराइन ही कहूँगा, हाँलांकि उनके सामने मैंने ऐसा कभी संबोधन नहीं किया था। हाँ, उनको चौधराइन और उनके पति को चौधरी जी के उपनाम से संबोधित करने के सिवाय मेरे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि मैंने उन पति और पत्नी दोनों के नाम जानने की कभी कोशिश ही नहीं की, क्योंकि इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी, समझने के लिए मैंने कभी अपने दिमाग का प्रयोग किया ही नहीं। परिस्थितियों के अधीन जो भी उपयुक्त लगा, कदम उठाया और आगे बढ़ता गया। खाई और पर्वत की कभी चिंता की ही नहीं।
चौधरी साहब का छोटा परिवार था। वे स्वयं, चौधराइन और उनके दो बच्चे सुमित और चंचल। सुमित जिसके नाम के प्रति मैं अपनी स्मरण शक्ति से पूरी तरह से निश्चित नहीं हूँ। सुमित मेरे विद्यालय में कक्षा 6 अ का विद्यार्थी था, जिस कक्षा का मैं कक्षाध्यापक भी था। उसी विद्यार्थी के कारण मेरी व्यवस्था उस घर में हुई थी। चंचल उसकी छोटी बहिन संभवतः तीसरी, चौथी या पाँचवी कक्षा की छात्रा रही होगी। चौधरी जी संभवतः एफसीआई के गोदाम में चौकीदार थे और उनकी ड्यूटी रात को रहती थी। मैं दिन में अपने विद्यालय में रहता था और वे दिन में सोते थे और रात को अपनी ड्यूटी पर रहते थे। उनको मैंने एक-दो बार ही देखा होगा। कभी किसी भी प्रकार की बातचीत भी हुई थी, मुझे स्मरण नहीं।
शैक्षणिक सत्र 97-98 में बेरोजगारी के उस दौर में भटकते हुए सरस्वती विद्या मन्दिर, शिकारपुर, उत्तर प्रदेश में टीजीटी हिंदी के रूप में कार्य करने का अवसर मिला था। शिकारपुर, जी हाँ, वही शिकारपुर जिसको लेकर मजाक उड़ाया जाता है। वैसे निजी विद्यालयों में सामान्यतः ग्रेड का कोई अधिक मतलब नहीं होता है, फिर भी उस विद्यालय में मेरी एक अनूठी स्थिति थी; साक्षात्कार के समय ही प्रबंधन ने स्पष्ट कर दिया था कि हम आपको टीजीटी का ग्रेड देंगे किंतु कक्षाएँ 12 वीं तक की पढ़वाएंगे। शिकारपुर से और क्या अपेक्षा की जा सकती थी? यथा नाम तथा गुण।
उसी विद्यालय में मेरे मित्र श्री विजय कुमार सारस्वत पहले से ही वाणिज्य पढ़ा रहे थे। उनके साथ भी यही हुआ था। प्रसन्नता के साथ स्वीकार करने के सिवा और कोई विकल्प नहीं था। बेरोजगार व्यक्ति के समक्ष अस्वीकार करने का विकल्प कहाँ होता है? उस विद्यालय में अगस्त 97 में काम करना प्रारंभ कर दिया था और अप्रैल 98 में छोड़ दिया था। इस दौरान श्री विजय जी के द्वारा सदैव ही सहयोग किया गया। वे वहाँ पहले से ही थे। अतः किराए पर कमरा दिलवाने का काम उन्होंने ही किया। सबसे पहले उन्होंने अपने मकान मालिक से कहकर अपने वाले मकान में ही कमरा दिलवाया। विजय जी की पत्नी उनके साथ रहती थीं। विजय जी के माता-पिता ने उन्हें स्पष्ट रूप से निर्देशित किया था कि खाने की व्यवस्था वे अपने आप ही करेंगे और मुझे खाना नहीं बनाने देंगे। विजय जी की पत्नी ने खाना बनाने की जिम्मेदारी स्वयं पर ही रखी। वहाँ ठीक ठाक ही चल रहा था किन्तु उस मकान मालिक को अकेले व्यक्ति का अपने यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता था। अपने अध्ययन को ध्यान में रखकर मैं विद्यालय से अवकाश अधिक लेता था। यह मकान मालिक महोदय को ठीक नहीं लगा और शीघ्र ही दूसरे मुहल्ले में दूसरा कमरा लिया गया और अपने आप खाना बनाने की व्यवस्था की।
नए कमरे पर आए हुए कुछ ही दिन हुए होंगे कि एक दिन कक्षा 6 के एक विद्यार्थी ने संपर्क किया कि आचार्य जी मम्मी ने भेजा है। उन्होंने पुछवाया है कि क्या आप मुझे ट्यूशन पढ़ा देंगे? उस विद्यालय में अध्यापक को आचार्य कहने की ही परंपरा थी। ट्यूशन पढ़ाना मेरी प्रवृत्ति में नहीं रहा। मैंने मना कर दिया कि मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाया करता। टालने के लिए सदभावना प्रकट करते हुए उससे कह दिया, ‘तुम्हें जरूरत हो तो वैसे ही शाम को आ जाया करो, तुम्हें बता दिया करूंगा।’
उस विद्यार्थी का नाम संभवतः सुमित था। पक्के तौर पर स्मरण नहीं। लगभग 27 वर्ष हो गए स्मृति धुँधली हो चुकी है। सुमित ने उसी शाम से आना प्रारंभ कर दिया। न चाहते हुए भी उसे पढ़ाना प्रारंभ करना पड़ा।
सुमित शाम को पढ़ने आता था। मेरा कमरा अत्यंत छोटा था और मेरा बिस्तर नीचे जमीन पर ही लगा होता था। बैठने के लिए चटाई व स्टूल कुछ भी नहीं था, कुर्सी की तो उस समय मैं, कल्पना ही नहीं कर सकता था। अतः रात को सोने और दिन में बैठने के लिए उसी बिस्तर का ही प्रयोग किया करता था। खाना बनाते समय ही उसे समेटा जाता था। एक-दिन कुछ रोटियाँ बच गईं थीं। मैंने सुमित को दे दीं कि वह अपनी भैंस को खिला दे। अगले दिन जब सुमित मेरे पास पढ़ने आया तो एक टिफिन में मेरे लिए खाना भी लेकर आया। मैंने चैककर पूछा, ‘खाना क्यों लाए हो?’
’मम्मी ने कहा है कि ऐसी रोटी खाकर तो आचार्य जी बीमार पड जाएंगे। आचार्य जी को खाना बनाना नहीं आता। उन्हें तू खाना खिलाकर आया कर।’ सुमित ने जबाब दिया। यह मेरे लिए अकल्पनीय था। बार-बार मना करने के बाबजूद वह नहीं माना और प्रतिदिन दोनों समय खाना लेकर आने लगा। ऐसे बार-बार आने से मुझे लगने लगा कि बच्चे का काफी समय बर्बाद होता है। अतः मैंने कहा, ‘बेटा! ऐसे बार-बार आने से समय खराब होता है। अपनी मम्मी से कहना कि यदि तुम्हारे घर में जगह हो तो मेरे लिए वहीं रहने की व्यवस्था कर लें। मैं यह कमरा छोड़कर तुम लोगों के यहाँ ही रह लूँगा।’
दूसरे दिन सुमित ने आकर बताया, ‘मम्मी ने कहा है, हम कमरा किराये पर नहीं उठाते। हमारे पास अच्छी व्यवस्था भी नहीं है। फिर भी आचार्य जी आकर हमारे मकान को देख लें। उन्हें ठीक लगेगा तो उनकी रहने की व्यवस्था अपने यहाँ कर लेंगे।’
मैंने उसके साथ जाकर देखा तो उनके मकान पर सीमेण्ट नहीं करवाया गया था। मकान ईंटों का था और नीचे कच्चा था। हाँ, बाहर वाले कमरे का एक दरवाजा बाहर खुलता था और एक अन्दर की और गैलरी में अंदर वे रहते थे और भैंस भी रखते थे। भैंस का दूध अपने लिए ही था, बेचने के लिए नहीं। संतोषी प्रवृत्ति का निष्कपट, निश्छल परिवार प्रतीत हुआ। ताम-झाम और प्रदर्शन से दूर। दो बच्चे थे- एक सुमित जो मेरी कक्षा में पढ़ता था और दूसरी उससे छोटी लड़की चंचल।
जब विजय जी से चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि आप जिस घर में जाने की बात कर रहे हो। उस चौधराइन से मुहल्ले में सभी लोग डरते हैं उसका व्यवहार अक्खड़ है। उनसे बचकर रहना ही उचित है। मैंने उनकी जाति तो पूछी ही नहीं थी। जाति-विरादरी पर मेरा कभी भी ध्यान नहीं जाता। मैं जाति भेदभाव को मानता ही नहीं। विजय जी की इस बात ने मुझे और भी स्पष्ट कर दिया। मैंने विजय जी से कहा, ’जो लोग ईमानदार प्रकृति के होते हैं। उनमें बनावटीपन और विनम्रता की कमी पाई जाती है। वे जैसा है, वैसा बोल देते हैं। उनके साथ सामान्यतः ऐसा ही व्यवहार होता है। लोग उनके साथ बैठने-उठने से डरते हैं। सच्चाई से सबको डर लगता है। आपके सिवा मेरा भी कोई मित्र नहीं है ना। इससे तो यही स्पष्ट होता है कि वह परिवार अच्छा है।
’मैंने अपनी बात कह दी है, आगे आपकी इच्छा। सोच-समझकर निर्णय करना।’ कहकर विजय जी चले गए। मेरे लिए कमरा बदलने का निर्णय थोड़ा मुश्किल हो गया।
जिस कमरे में मैं रह रहा था, उसके मकान मालिक एक डाक्टर थे। डिग्री का तो पता नहीं किंतु वे वहीं कहीं स्थानीय प्रैक्टिस करते थे। ऐसा मेरी जानकारी में था। मुझे भी कुछ अस्वस्थता थी। मेरे सीने में दर्द की शिकायत हो रही थी। मैंने उनसे चर्चा की तो उन्होंने कहा। रविवार को मैं अपनी पत्नी को लेकर खुर्जा जा रहा हूँ। आप भी साथ चले चलना। ऐक्सरे करवा लेना। उनकी पत्नी अस्वस्थ भी हैं, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं था। मैं रविवार को उनके साथ चल पड़ा। उनकी बातचीत से उनका व्यवहार अजीब सा लग रहा था। किसी भी प्रकार की बीमारी की बातचीत नहीं हुई।
खुर्जा जाकर डाक्टर साहब के कहने पर मैंने अपना एक्सरा कराया। वहाँ जाकर पता चला कि उन्होंने अपनी पत्नी का अल्ट्रासाउंड कराया था। रास्ते में उन्होंने मुझे कहा कि किसी को बताना मत कि मैंने अपनी पत्नी का अल्ट्रासाउंड करवाया है। अगले सप्ताह ही वे अपनी पत्नी को गर्भपात के लिए लेकर गए। मुझे यह सब अनुचित व गैर कानूनी लग रहा था। किंतु मैं कुछ भी करने की स्थिति में नहीं था। अतः मुझे कमरा बदलने का निर्णय तुरंत करना पड़ा और मैं उस कमरे को छोड़कर चौधराइन के घर में आ गया। चौधराइन के घर मेरा कोई कमरा नहीं था। बाहरी कमरे में मेरे और सुमित के सोने की व्यवस्था की गई थी। मैं खाट पर सोना पसंद नहीं करता था। अतः मेरी वजह से दो तख्त खरीदे गए। एक मेरे लिए और एक सुमित के लिए। बिस्तर लगाने से लेकर, कपड़े धोने सहित खाना खिलाने तक की समस्त जिम्मेदारियाँ चौधराइन ने अपने ऊपर ले लीं थीं।
चौधराइन का मकान भले ही छोटा था, तामझाम और प्रदर्शन की भावना न होने के कारण आकर्षक भी न था किंतु उनका निश्छल, पवित्र प्रेम, निष्कपटता व सहयोग आज तक मुझे और कहीं देखने को नहीं मिला। जिस तरह सुविधापूर्वक वहाँ रहा, उस तरह सुविधापूर्वक आवास मेरी माताजी और पत्नी के साथ भी नसीब नहीं हुआ। चौधराइन की प्रत्येक माँ की तरह केवल अपने बेटे की पढ़ाई की अपेक्षा थी, जो मेरे लिए विशेष बात न थी। कितना किराया, खाने के कितने रुपए, दूध का हिसाब किताब वहाँ चर्चा का विषय कभी न बना। खर्चे सदैव मेरी अपेक्षा से कम ही रहे। परिवार की तरह ही नहीं परवार के सदस्य के रुप में सही अर्थो में मैं वहाँ रहा। कोई जिम्मेदारी नहीं, सभी प्रकार की देखभाल। इस तरह की कल्पना भी करना मेरे लिए संभव नहीं था।
व्यक्तिगत रूप से खान-पान में मेरी कोई विशेष माँग नहीं रहती। चौधराइन के द्वारा स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही भोजन बनाया जाता था। हम भले ही शिकारपुर कस्बे रह रहे थे, किंतु चौधराइन के यहाँ ग्रामीण रहन-सहन था। जो मुझे अत्यन्त प्रिय था। अपनापन था। हरी सब्जी अक्सर रहती थी। हरी सब्जी में घी डालना वे कभी नहीं भूलतीं थीं। घी के बिना हरी सब्जी खाना उनके लिए अशुभ था। वे दूध नहीं बेचतीं थीं किंतु मुझे दूध पिलाने की व्यवस्था उन्होंने स्वयं ही स्वीकार कर ली थी। उस समय मैं संभवतः आधा लीटर दूध की कीमत दिया करता था। मैं अक्सर पढ़ने-लिखने में दूध पीना भूल जाया करता था। वे कई-कई बार दूध गरम करके लाया करतीं थीं, क्योंकि ठण्डा दूध पिलाना उनको स्वीकार नहीं था, और मैंने अपने खान-पान पर कभी ध्यान दिया ही नहीं, उस समय दूध पर ही क्या देता?
मेरे और अपने बेटे के पढ़ने के लिए उन्होंने गैस का छोटा पेट्रोमेक्स खरीदवाया था। बाद में दूध ठण्डा न हो जाय, इसे ध्यान में रखकर वे कई बार दूध के बर्तन को भी पेट्रोमेक्स के ऊपर रख दिया करतीं थीं। मुझे ध्यान नहीं देना था, नहीं दिया और अक्सर दूध की रबड़ी बन जाया करती थी। वे इतने पर भी कभी गुस्सा नहीं हुईं। पानी के बिना दूध केवल और केवल वहीं पीने को मिला। मेरी माताजी ने भी कभी मुझे बिना पानी का दूध नहीं पिलाया होगा। दूध बेचने वालों के यहाँ तो शायद भैंस और गाय ही दूध में पानी मिला दिया करती हैं अर्थात् बिना पानी का दूध मिलना लगभग असंभव है। रहीं सही कसर घर की महिलाएँ माँ, बहिन, पत्नी कोई भी हों, पूरी कर देती हैं। चौधराइन के लिए दूध का मतलब दूध था। पानी मिलाने का कोई मतलब ही नहीं।
चौधराइन लोभ-लालच से पूर्णतः मुक्त थीं। मैंने कभी उन्हें किसी प्रकार की शिकायत करते नहीं सुना। एक बार की बात है। उनके पति ने एक नई साइकिल खरीदी। वे शाम को नई साइकिल को लेकर अपनी ड्यूटी करने गए। सुबह जब आए जो उनका मुँह लटका हुआ था। उनके चेहरे से ही चिंता व निराशा झलक रही थी। चौधराइन ने मुस्कराकर पूछा, ‘क्या हुआ? इस प्रकार चेहरे पर बारह क्यों बजे हुए हैं?’
‘किसी ने मेरी साइकिल चुरा ली। चौधरी साहब ने डरते हुए बताया।’ ऐसी स्थिति में कोई भी पत्नी अपने पति पर आग-बबूला हो उठती, किंतु चौधराइन तो चौधराइन थीं। उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, ‘इसमें सुस्त होने की क्या बात है? साइकिल एक दिन पुरानी हो गई थी। अब नई साईकिल खरीद लेना।’
इस तरह प्रसन्नता बिखेरने वाली महिला अपवाद स्वरूप हीं कहीं मिलेंगीं। सामान्यतः पति-पत्नी एक-दूसरे पर ताना कसने, व्यंग्य करने के अवसर ढूढ़ते हैं। सामान्यतः स्त्रियाँ खाना परोसकर खिलाने के लिए सामने बैठ जाती हैं और दिनभर की समस्याएँ सुनाना प्रारंभ कर देती हैं। अनजाने में ही वे पूरे प्रयास करती हैं कि सामने वाला खाना खा नहीं ले। उसे इतने तनाव देने की कोशिश करती हैं कि या तो वह खाना खाए ही नहीं, खा भी ले तो उसका पाचन तंत्र तनाव के कारण उसे पचा नहीं पाए।
चौधराइन बिल्कुल इसके उलट थीं। वे बड़े ही प्रेम से प्रसन्नतापूर्ण वातावरण बनाकर खाना खिलाया करती थीं। दोपहर को विद्यालय से वापस होते-होते मैं अक्सर तनाव में होता था। जवान खून था। तभी-तभी काम करना शुरू किया था। विद्यालय में विद्यार्थियों से अपेक्षित व्यवहार न पाकर मैं तनाव में ही वापस लौटता था। मेरी आदत रही है कि तनाव की स्थिति में मैं खाना नहीं खाता। वे मेरे और अपने बेटे के विद्यालय से वापसी की प्रतीक्षा कर रही होती थीं। उनका बेटा मुझसे पहले घर पहुँच जाया करता था। उसे मेरे पहुँचने से पूर्व ही खाना खिला चुकी होती थीं। मेरे पहुँचने पर उनका कहना होता, ‘आचार्य जी, मुँह-हाथ धो लीजिए। मैं खाना लगा देती हूँ।’
तनाव में रहने के कारण मेरा जबाब अक्सर यही रहता था, ‘मुझे खाना नहीं खाना।’
‘ठीक है कोई बात नहीं। आप मुँह हाथ धोकर बैठिए तो सही।’ यह कहकर वे मेरे पास ही बैठ जाया करतीं और सामान्य बातचीत करते हुए ऐसी बातें करतीं कि मुझे हँसी आ जाती। हँसी आने का मतलब तनाव का गायब होना। इसके बाद मुझसे कहतीं कि अब तो खाना खा लीजिए। मेरे पास खाना खाने के सिवाय और कोई विकल्प बचता ही कहाँ था। इस तरह प्रसन्नता और खाना दोनों एक साथ परोसने वाली देने वाली चौधराइन को भूलाया जाना संभव नहीं है।
चौधराइन अत्यंत लगलशील व परिश्रमी थीं। जो ठान लिया, उसे पूरा करके ही छोड़ना है। एक बार मेरे लिए स्वेटर बनाने का काम हाथ में लिया। स्वेटर के लिए ऊन खरीदकर लाईं। बुनना प्रारंभ कर दिया। दीपावली आने वाली थी। मैंने विद्यालय में बात करके दीपावली के लिए अवकाश स्वीकृत करा लिए और उन्हें शाम को बताया कि मैं कल अपने घर जाऊँगा। उनका स्वेटर अभी पूरा नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, ‘आप अपनी मम्मी के पास जा रहे हो। यह स्वेटर तो आपको पहनाकर ही भेजूँगी। भले ही मुझे पूरी रात जागकर बुनना पड़े और संकल्प की धनी चौधराइन ने मुझे दूसरे दिन स्वेटर पहनाकर ही घर रवाना किया।’
चौधराइन आज भी मेरी स्मृतियों में हैं। हों भी, क्यों ना? वे थी ही विलक्षण व्यक्तित्व की धनी। वे पढ़ी-लिखी थी या नहीं? मुझे नहीं पता किंतु वे शिक्षित और सुसंस्कृत अवश्य थीं। यह उनके व्यवहार से ही प्रमाणित था। चौधराइन की तरह की विलक्षण व अप्रतिम महिला मैंने कोई दूसरी नहीं देखी। चौधराइन और उनका छोटा सा अनूठा प्रेम भरा वह परिवार मुझे आज भी याद है। उस घर में मैंने कभी चौधरी साहब को भी क्रोध में नहीं सुना। सुमित को भी डाँटने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। हाँ! चंचल बिटिया में अवश्य ही बालसुलभ चंचलता थी। इच्छा होती है कि सुमित के समाचार लेने वापस शिकारपुर जाकर देखूँ। मैंने कई बार वहाँ जाने की योजना बनाई भी किंतु मेरे मित्र विजय जी ने मुझे बाद में बताया था कि वे अपना मकान बेचकर कहीं और चले गए हैं। बिना नाम पते के उन तक पहुँचना असंभव सा जानकर सुमित के समाचार जानने के प्रयत्न छोड़ने पड़े।