मनुष्य स्वभाव से ही जिज्ञासु है। वह ज्ञान पिपासू है। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि वह ज्ञान-पिपासू है, इसीलिए मनुष्य है। ‘आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्।’ अर्थात खान-पान, नींद, संतति उत्पत्ति के स्तर पर पशु और नर में कोई भेद नहीं है। जीव विज्ञान की दृष्टि से मानव भी एक प्राणी है। मानव की जिज्ञासा की प्रवृत्ति ही उसे खास बनाती है। अपनी जिज्ञासा की संतुष्टि के लिए वह विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त होने वर वह अपने आचरण में परिवर्तन लाकर अपने आपको प्रकृति, पर्यावरण व अन्य प्राणियों के अनुकूल बनाकर अपना व सभी प्राणियों का हित सुनिश्चित करता है। सभी के हित में अपना हित खोजने के कारण ही मानव और मानवीयता का सिद्धांत स्थापित होता है। प्रत्येक मनुष्य स्वयं को ज्ञानी बनाना चाहता है या कम से कम अज्ञानी होते हुए भी अपने आपको ज्ञानी समझता है। सुकरात के अनुसार, वास्तव में ज्ञानी वह है, जो यह जान ले कि वह कुछ नहीं जानता। उसे हर क्षण जिज्ञासु बने रहकर सीखना है। हर क्षण सीखना है। हर प्राणी से सीखना है। हर वस्तु से सीखना है। सीखना ही मानव जीवन का सार है। सीखने का आशय कुछ जान लेने मात्र से नहीं है, सीखने का आशय उसका उपयोग करके अपने आचरण में सुधार करना है।
ज्ञान प्राप्त करना या सीखना इतना महत्वपूर्ण है तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सीखने में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ज्ञान प्राप्ति का मार्ग कौन सा है? स्वामी विवेकानन्द के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के अनेक मार्ग नहीं हैं, जिनमें से किसी एक को चुना जा सके। ज्ञान प्राप्ति के लिए केवल एक ही मार्ग है- ‘एकाग्रता।’ एकाग्रता ही सीखने का आधाभूत तत्व या मार्ग है। एकाग्रता के बिना सीखना संभव नहीं है। सीखने के बिना किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना संभव नहीं है। अतः यह भी कहा जा सकता है कि सफलता का एकमेव मार्ग एकाग्रता है। एकाग्रता ही वह शक्ति है जो ज्ञान प्राप्ति को संभव बनाती है। जिसमें यह शक्ति जितनी अधिक होगी, वह उतनी अधिक कुशलता प्राप्त करने में सफल होगा। वह भले ही विद्वान अध्यापक हो, मेधावी छात्र हो, चर्मकार हो, रयोइया हो; कोई भी हो एकाग्रता ही वह शक्ति है, जो उसे उसके हुनर में पारंगत बनाएगी।
पशु में एकाग्रता की शक्ति कम होती है। जो पशुओं को सिखाने का काम करते हैं, वे इस कठिनाई का अनुभव करते हैं। सबसे निम्न मनुष्य की उच्चतम पुरुष से तुलना करो। उन दोनों में केवल एकाग्रता की मात्रा का ही अन्तर मिलता है। किसी भी कार्य की सफलता इसी पर निर्भर करती है। ओशो तो ध्यान को भी इसी प्रकार परिभाषित करते हैं। उनके अनुसार ध्यान का आशय केवल कुछ घण्टे आँख बन्द करके अपने इष्ट का ध्यान लगाना नहीं है। ध्यान का आशय अपनी प्रत्येक गतिविधि को भले ही खाना खाना हो, सोना हो, खेती करना हो, पति-पत्नी के साथ एकान्तिक क्षणों का आनन्द हो, अध्ययन या अध्यापन हो आदि सभी क्रियाओं को पूर्ण ध्यान के साथ करना अर्थात एकाग्रता के साथ करना ही सच्चा ध्यान है। जो व्यक्ति अपने संपूर्ण समय में की जाने वाली समस्त गतिविधियों को ध्यानपूर्वक करता है। वही सच्चा ध्यानी है। वास्तव में इस प्रकार ध्यान करने वाला व्यक्ति प्रत्येक गतिविधि में एकाग्रता के कारण प्रत्येग गति विधि में सफलता प्राप्त करने का अधिकारी है। कारण-कार्य सिद्धांत के अनुसार प्रकृति के नियमानुसार उसे सफलता ही मिलती है।
एकाग्रता की बात करना सरल मालुम पड़ता है, किन्तु एकाग्रता का अभ्यास अत्यन्त कठिन है। स्वामी विवेकानन्द के अनुसार, जब कभी व्यक्ति सब चिन्ताओं को छोड़कर ज्ञान-लाभ के उद्देश्य से मन को किसी विषय पर स्थिर करने का प्रयत्न करता है, त्यौं ही मस्तिष्क में सहस्रों अवांछित भावनाएँ दौड़ आती हैं, हजारों चिंताएँ मन में एक साथ आकर उसको चंचल कर देती हैं। किसी प्रकार रोककर मन को वश में लाया जाए, यही राजयोग का एकमात्र आलोच्य विषय है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा व समाधि आदि सभी एकाग्रता का संधान करने के ही उपकरण हैं। एकाग्रता के लिए स्वामी जी ब्रह्मचर्य की आवश्यकता पर जोर देते हैं। उनके अनुसार सभी अवस्थाओं में मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना ही ब्रह्मचय कहलाता है। उनके अनुसार अपवित्र कल्पना भी उतनी ही बुरी है, जितना अपवित्र कार्य। वास्तविकता यही है कि विचार ही मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। विचार ही कार्य में परिणत होते हैं। अतः यदि कल्पना अपवित्र होगी तो कर्म भी अपवित्र हो ही जाएंगे।
एकाग्रता के लिए श्रद्धा की भी आवश्यकता होती है। आत्मविश्वास और श्रद्धा के बिना हम किसी विषय पर स्थिर रह ही नहीं सकते। स्वामी विवेकानन्द के गुरु श्री रामकृष्ण कहा करते थे, ‘जो अपने को दुर्बल समझता है, वह दुर्बल ही हो जाता है।’ वास्तव में मनुष्य जैसा सोचता है, वैसा ही बन जाता है। विचार ही कर्म का रूप लेकर परिणाम में परिणत होता है। यदि हम सोचें कि हम कुछ हैं, हममें शक्ति है तो हममें सचमुच ही शक्ति आ जाएगी। एकाग्रता ही ज्ञान, जीवन, शक्ति और आध्यात्मिकता सहित सभी विषयों की मूल है। एकाग्रता के बिना हम प्रभावी रूप से कोई कार्य नहीं कर सकते और कार्य के बिना परिणाम प्राप्ति की कल्पना करना ही मूखर्ता है। अतः हमें यह स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए कि एकाग्रता ही ज्ञान व सफलता प्राप्ति का एकमात्र उपकरण है।
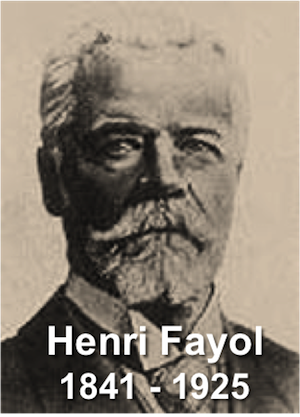





कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें