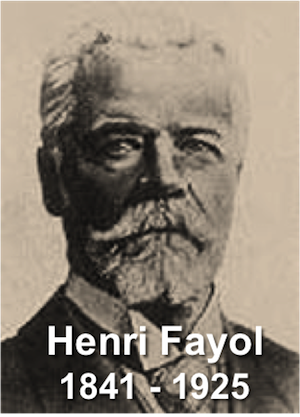सामान्यतः स्वार्थ को बड़े ही संकीर्ण और नकारात्मक अर्थ में लिया जाता है। स्वार्थ के अन्य पर्यायवाचियों में, खुदगर्ज, मतलबी, प्रयोजनवादी के साथ-साथ स्व-केन्द्रित और आत्मोत्कर्ष के लिए काम करने वाला व्यक्ति भी इसी अर्थ में लिया जाता है। सामान्य जन स्वार्थी व्यक्ति कहने से अपने आपको अपमानित महसूस करते हैं। हम दिन-रात अपने स्वार्थ के लिए आपा-धापी में लगे हैं। अपने आपको भुलाकर भी अपने स्वार्थो को पूरा करने के लिए लगे रहते हैं। हम अपने आस-पास ध्यान से देखें तो हमारी सभी गतिविधियाँ स्वार्थ पर ही केन्द्रित होती हैं। स्वार्थ ही हमारा सबसे अच्छा प्रेरक है, किन्तु इसके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण अपने स्वार्थ के लिए मार-काट करने वाला व्यक्ति भी अपने आपको स्वार्थी कहलाना पसंद नहीं करता। हम अपने स्वार्थो का महिमामंडन करते हुए उन पर परोपकार या समाजसेवा का आवरण डालने का प्रयत्न करते रहते हैं। हम इसे स्वीकार नहीं कर पाते कि स्वार्थ सभी गतिविधियों में व्याप्त है। विकास की प्रक्रिया के लिए स्वार्थ आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है।
स्वार्थ की नकारात्मकता स्वार्थ के वास्तविक अर्थ पर विचार न करने के कारण स्थापित हो गई है। वास्तविकता इससे भिन्न है। स्वार्थ व्यापक रूप से हर जगह और हर काल में मौजूद है। स्वार्थ व्यक्तियों को अपनी जरूरतों और इच्छाओं को दूसरों की तुलना में प्राथमिकता देने का नाम है। यह एक स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है। स्वार्थ मानव स्वभाव का एक अभिन्न व अनिवार्य घटक है। यह जीवन के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। व्यक्तिगत अस्तित्व, सुरक्षा और विकास के लिए स्व-हित की एक मजबूत भावना को होना अत्यंत आवश्यक है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने मैत्रैयी से कहा था, ‘‘न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवित, आत्मनस्तु’’ अर्थात जैसे पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है, उसी प्रकार पत्नी भी अपने पति से प्रेम करती है, लेकिन यह प्रेम पति के प्रति नहीं, बल्कि अपने आत्म के प्रति होता है। इसी श्रंखला में महर्षि याज्ञवल्क्य के विचार को आगे बढ़ाते हैं कि संसार के सभी संबन्ध स्वार्थ पर आधारित हैं। हम सभी एक-दूसरे के साथ रहकर एक-दूसरे का सहयोग करके वास्तविक रूप से अपने स्वार्थ को ही साध रहे होते हैं। व्यक्तिगत, पारिवारिक व सामाजिक संबन्ध पारस्परिक स्वार्थ के लिए ही होते हैं। हमें इस वास्तविकता को स्वीकार करने की आवश्यकता है।
हमारा प्रत्येक विचार, हमारी प्रत्येक गतिविधि, हमारा प्रत्येक संबन्ध कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी स्वार्थ, किसी न किसी कामना, किसी न किसी आवश्यकता या किसी न किसी इच्छा की पूर्ति के लिए ही होता है। हम अपने परिवार, समाज, देश के लिए काम करने का दंभ भरते समय भी अपने आपको महान सिद्ध करने और प्रतिष्ठा प्राप्त करने की भावना के वशीभूत होते हैं। परमार्थ भी वास्तव में किसी न किसी रूप में स्वार्थ का ही अंग होता है। अध्यात्म भी आत्म विकास के लिए ही होता है। भक्ति भी स्व-हित के लिए ही होती है। मुक्ति या मोक्ष की कामना भी अपने लिए ही होती है। स्वार्थ ही व्यक्ति को कर्तव्यशील व कर्मठ बनाता है। हमारे सामने समस्या यह है कि हम सभी अपने-अपने स्वार्थो के लिए काम करते हैं किंतु इस तथ्य को स्वीकार करने का साहस नहीं कर पाते। हम नितांत स्वार्थी होते हुए भी अपने आपको समाजसेवक और परमार्थी दिखलाने का आडंबर करते हैं और तनाव में जीते हैं।
भक्त कवि तुलसीदास जी की कृति रामचरितमानस भक्ति साहित्य में अप्रतिम स्थान रखती है। विश्व की अनेक भाषाओं में अनुदित होते हुए वह एक प्रमुख धर्म-ग्रन्थ के रूप में स्थापित है। ध्यान देने वाली बात है कि गोस्वामी तुलसीदास ने उसके सृजन के फलस्वरूप अपने आपके लिए महानता का आडंबर नहीं पाला। ‘स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा।’ कहकर उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वे उसकी रचना स्वान्तः सुखाय अर्थात अपने आनन्द के लिए या अपने सुख के लिए कर रहे हैं। उन्होंने अपने आपको स्पष्ट रूप से स्वार्थी स्वीकार किया। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि उनके स्वान्तः में सभी का आनन्द समाहित हो गया। अब बहुत बड़ी जनसंख्या रामचरितमानस के पाठ से आनन्दानुभूति करती है। जब हमारा स्वार्थ सामाजिक हितों को हानि नहीं पहुँचाता, तभी वह वास्तव में सच्चा स्वार्थ है। किसी के हितों को हानि पहुँचाकर हम अपना स्वार्थ नहीं साध सकते। किसी के हितों को हानि पहुँचाना हमें मानसिक रूप से अशांत, ग्लानि, तनाव और असुरक्षा से भर देगा। हम सदैव आशंकाओं का सामना करेंगे, यही नहीं, जिसके हितों को हानि पहुँचेगी, वह हमारे हितों को हानि पहुँचाएगा। इस प्रकार हमारा जीवन तनाव व संकटों का सामना करेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि हमारा स्वार्थ सभी के स्वार्थ में ही है अर्थात परमार्थ भी हमारे स्वार्थ का ही घटक है। अपने पड़ोसियों को असंतुष्ट कर हम संतुष्ट नहीं रह सकते। पड़ोसियों को असुरक्षित कर हम भी सुरक्षित नहीं रह सकते।
अपने जीवन को सुखद, शांतिपूर्ण व आनंदित बनाने के लिए इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि हम सब स्वार्थी हैं। हमारे सभी संबन्ध स्वार्थ पर आधारित हैं। हमारे स्वार्थ को पूरा करने के लिए हमें दूसरों के सहयोग की आवश्यकता है। दूसरा हमारे स्वार्थ को पूरा करने में तभी सहयोग करेगा, जब हम उसके स्वार्थ को पूरा करने में सहयोग करेंगे। यही सहकारिता का मूल है। ‘एक सभी के लिए और सब एक के लिए’ इस मूलमंत्र को स्वीकार करके ही हम अपने-अपने स्वार्थाे को पूरा कर सकते हैं और सभी अपनी-अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए साथ-साथ जी सकते हैं। इसी पथ पर चलकर हम विकास पथ पर अग्रसर हो सकते हैं।
हमंे इस यर्थार्थ को समझना होगा कि पति अपनी पत्नी को प्रेम निस्वार्थ भाव से नहीं करता, स्वार्थ भाव से करता है। पत्नी भी पति को अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए ही प्रेम करती है। दोनों की कामनाओं की पूर्ति एक-दूसरे से होनी है, दोनों को एक-दूसरे की आवश्यकता है; इसी कारण एक-दूसरे को प्यार करने और सात जन्म तक साथ निभाने का प्रदर्शन किया जाता है अन्यथा की स्थिति में एक-दूसरे को मारकर कई टुकड़ों में काटकर इधर-उधर फेंकने सूटकेसों में बन्द करने या नीले ड्रम में पैक करने के उदाहरण सामने आ रहे हैं। माता-पिता बच्चे को जन्म देने और लालन-पालन करने का काम बच्चे को प्रेम करने के कारण नहीं, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए ही करते हैं। उन्हें यह विश्वास होता है कि वे अब बच्चों का लालन-पालन कर रहे हैं, बच्चे उनकी वृद्धावस्था में उनकी देखभाल व सेवा करेंगे। यही नहीं समाज में बच्चों से माता-पिता की इज्जत बढ़ाने और उनके नाम को रोशन करने की अपेक्षा भी की जाती है अन्यथा की स्थिति में माता-पिता द्वारा आनर किलिंग भी कर दी जाती हैं। संताने भी माता-पिता की हत्या करने में पीछे नहीं रहतीं। संपत्ति के लिए निकटतम संबन्धियों की हत्याओं के प्रकरणों से इतिहास भरा पड़ा है। वर्तमान में भी अखबारों में इस प्रकार की घटनाओं का अभाव नहीं रहता। हमें काल्पनिक आदर्शवाद के अन्तर्गत परमार्थ की अवधारणा से अलग हटकर यथार्थ को स्वीकार करने की आवश्यकता है कि दुनिया स्वार्थ पर ही टिकी है। स्वार्थ ही विकास का आधार है। हाँ! स्वार्थ की व्यापकता को समझकार इसे सकारात्मक अर्थ में लेने की आवश्यकता है।
स्वार्थ नकारात्मक शब्द नहीं है। स्वार्थ सकारात्मक है और विकास का आधार है। स्वार्थ ही हमें हमारी गतिविधियों का करने की प्रेरणा देता है। स्वार्थ ही वह आधार है, जो हमें काम करने, संबन्ध बनाने, परिवार व समाज का गठन करने, प्रेम करने, सम्मान करने, पूजा करने; यहाँ तक कि समर्पण और आत्मोत्सर्ग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। स्वार्थ के बिना व्यक्ति कर्म से विरत हो सकता है। स्वार्थ न केवल व्यापक है, वरन यह मानवता और सृष्टि के विकास के लिए आवश्यक और अनिवार्य भी है। अतः आइए स्वार्थ के महत्व को समझते हुए हम स्वार्थी बनें और विकास के पथ पर बढ़ें।